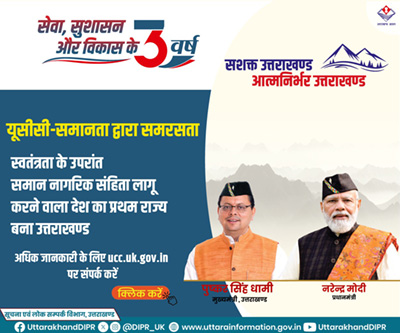डॉ मनोज तत्वादी
लेखक भारतीय पारस्थितीकी एवं पर्यावरण संस्थान के पूर्व छात्र एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सामजिक संगठनो से जुडे है. वर्तमान में भारतीय जन-संचार संस्थान-आई.आई.एम.सी. (पश्चिमी क्षेत्र) व युनिसेफ के प्रकल्प समन्वयक है.
प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका ‘नेचर’ में प्रकाशित एक शोध के अनुसार हाल ही में दर्ज किए गए तापमान परिवर्तन के ‘पैटर्न’ पिछले 24000 वर्षो की तुलना में अप्रत्याशित एवं चिंताजनक भी है. एरिझोना विश्वविद्यालय के इस शोध से मुख्यत: 3 परीणाम प्रमाणित हुए है-
- आखिरी हिम युग (आईस ऐज) के बाद वातावरण परिवर्तन के प्रमुख कारक है- हरितगृह वायु के वार्षिक उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैसो के वार्षिक उत्सर्जन में वृद्धी) में वृद्धी एवं ध्रुवीय हिम आच्छादन में कमी.
- पिछले 10000 वर्षो से वैश्विक वातावरण में तापमान के लगातार बढने का क्रम.
- पिछले 150 वर्षो की ग्लोबल वार्मिंग बढने की दर एवं व्यापकता ( रेट एंड मैग्नीट्युड) इन मापदंडो पर विगत 24000 वर्षो की तुलना में ज्यादा है.
ऐसे ही अनेक वैज्ञानिक शोध बार-बार खतरे की घंटी बजा कर मानव-निर्मित मानव जाती के आगामी विनाश के बारे में आगाह कर रहे है. औद्योगीकरण की अन्धाधुंध प्रगती एवं विश्व-सिरमौर बनने की अंतर्राष्ट्रीय राजनीती जहा पहुंच कर शांत होती है वह धाम है वैज्ञानिको की प्रयोगशाला ! यहां से प्रसृत निष्कर्ष दोनो की रफ्तार नियंत्रित करने एवं नकेल कसने की ताक़त रखते है. अतीत की जाने-अनजाने में की गई गलतियो पर वैज्ञानिक-संशोधन के परिणाम वर्तमान में वैश्विक परिषद में गंभीर चिंतन करने को बाध्य करते है. इसी कडी में स्कॉटलंड के शहर ग्लास्गो में 31-आक्टोबर से 14 -नवंबर याने दो सप्ताह के महा-मंथन के पश्चात संपन्न सीओपी 26 (कन्फरेंस ऑफ पार्टीज टू यु.ए.न फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ओन क्लायमेट चेंज का 26 वा) संमेलन था जिसमे विश्व के लगभग 100 से अधिक देशो का सहभाग था.
समझौते के मुख्य बिंदू
- पूर्व-औद्योगिक काल से ग्लोबल-वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सिअस तक सीमित रखना.
- जीवाश्म-इंधन (फ़ॉसिल फ्युल) पर दी जाने वाली अनुपयुक्त सबसिडी को बंद करना एवं जीवाश्म-इंधन का उपयोग पुरी तरह से बंद करने की बजाय चरण-बध्द तरीके से उपयोग कम करना. यह कोयले के इस्तेमाल को चरण-बध्द तरीके से कम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है.
ग्लासगो समझौते में सन 2030 तक इन उद्देश्यो की पूर्ती हेतू प्रयासो को अधिक नियोजित, कटिबद्ध एवं सुनिश्चित करणे पर बल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से सन 2023 में सर्व सदस्यीय सभा बुलाने की आवश्यकता को भी अधोरेखित किया गया है.
बिन पैसे सब सून
सन 2001 में विकसित देशो ने सन 2020 तक, प्रती वर्ष 100 बिलियन डॉलर की निधी उपलब्ध करावाने का संकल्प लिया था. पेरीस समझौते में इस संकल्प को सन 2025 तक के लिए बढा दिया था. किंतु, वह 100 बिलियन का वादा पूरा न हुआ ! कारण? खैर जाने भी दिजीये! अब तसल्ली की खबर यह है इस बार यह तय हुआ है की सन 2023 तक पुराने वादो की पूर्तता की जाएगी.
विकसित देशो पर एक सर्वमान्य व घोषित नैतिक जिम्मेदारी है वैश्विक पर्यावरण को सुधारने के प्रयासो में पहल लेने की. कारण? उत्तर के रूप में सदाबहार पुराने गाने की एक लाईन ही काफी है की- ‘तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना , गरीब जान के’. पर्यावरण असंतुलन की मार सबसे अधिक सहन करते है छोटे, आर्थिक दुर्बल एवं द्वीप- देश ! पर्यावरण-असंतुलन से उपजी आपदा से निपटने हेतू आज भी ऐसे संस्थागत ढांचे का अभाव है जो विकट समय में राहत सामग्री ,आर्थिक-सहायता के साथ पिडीत देश तक पुनर्वसन को योजना बध्द तरीके से पहुचाना सुनिश्चित करे. आपदा के कारण हुए नुकसान इस मद को 8 वर्ष पूर्व वारसॉ संमेलन में शामिल किया गया था. ग्लास्गो में इस अहम मुद्दे पर सिर्फ चर्चा हुई किंतु ठोस निर्णय नही आया. यह बात इस संमेलन के मुख्य अपयशो में से एक है. विकासनल देशो ने सन 2021 में आर्थिक दुर्बल एवं छोटे देशो के लिए 15 बिलियन डॉलर की निधी एकत्रित की थी. इस संमेलन में सन 2025 से इस राशी को दुगुना करने का संकल्प लिया गया. इस प्रस्ताव का पारित होना भी इस संमेलन की सफलता का चरण माना जा रहा है.
कार्बन पद-चिन्ह के अच्छे दिन
संक्षेप में कहे तो पर्यावरण में घातक उत्सर्जन में मान्य तरीको से कमी लाने पर उद्योग को कार्बन क्रेडीट प्राप्त होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विनिमय किया जा सकता है. क्योतो प्रोटोकोल के अंतर्गत ऐसा कार्बन मार्केट उपलब्ध था किंतु पेरीस समझौते के तहत प्रक्रिया व नियमो में स्पष्टता के अभाव में कार्बन मार्केट कार्यशील नही हो रहा था. विकसित देशो ने उनके उत्सर्जन लक्ष्यो के प्रती लापरवाही बरतने के कारण विकासशील देश जैसे भारत, चीन व ब्राजील के पास कार्बन क्रेडीट प्रचुर मात्रा में जमा हो गये. दो संमेलनो के एक ही विषय पर पृथक-पृथक गाईड लाईन्स एवं उसके कारण उपजे संभ्रम के कारण कार्बन क्रेडीट के वैश्विक विनिमय के अवरोध जैसे महत्त्वपूर्ण विषय को सुलझाने का संपूर्ण श्रेय ग्लास्गो संमेलन को जाता है. यह इस संमेलन की प्रमुख सफलताओ में से एक है.
जिन खोजा तिन पाईयाँ
कुल जमा, इस संमेलन से पर्यावरणविदो को विशेष प्रसन्नता नही मिली. जैसे अमेरिका की प्रिंसटन युनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक माइकल ओप्पेनहीम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की, “ 1.5 डिग्री सेल्सिअस का लक्ष्य ग्लास्गो संमेलन से पहले ही खत्म होने की कगार पर है और अब इसे मृत घोषित करने का समय आ गया है.” इसी तरह जर्मन अनुसंधानकर्ता एच.ओ. पोर्टनर के अनुसार,” ग्लास्गो संमेलन में काम किया गया लेकीन पर्याप्त प्रगति नही हुई.” अर्थात, इन मतो को मान्यता देने वाले वर्ग का मानना है की इस शीर्ष संमेलन में पर्यावरण के विषय में कठोर एवं कारगर उपायो के क्रियांवयन पर निर्णय लेना चाहिये था.
वही दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख पेत्रीसिया एस्पीनोसा ने कहा की, ” संयुक्त राष्ट्र की गणना के अनुसार, १.५ डिग्री सेल्सिअस का लक्ष्य हासील करने के लिए उत्सर्जन को सन 2030 तक आधा करने की आवश्यकता है, लेकीन यह सन 2010 के बाद से करीब 14 प्रतिशत बढा है.” साथ ही, सी ओ पी 26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने भी संमेलन में सर्व सदस्यो की सहभागीता, सहयोग एवं सफलता पर समाधान व्यक्त किया है. जी हां, ये वही आलोक शर्मा है जिनका जन्म आगरा(उ.प्र) में हुआ और बाद में ब्रिटिश नागरिक बने. चर्चा में खासकर तब आए जब सन 2019 में इन्होने हाउस ऑफ कॉमन में सांसद बनते समय पद और गोपनीयता की शपथ हाथ में श्रीमद् भगव्द्गीता रख कर ली थी.
संमेलन के पक्ष-विपक्ष का विवाद दरकिनार कर कहा जा सकता है की बावजूद सभी कामियों-खामियों के, ऐसे वैश्विक संमेलन और उस निमित्त से हर बार अतीत में की गई गलतियो की जुगाली एवं भविष्य को भीषण विभिषिका से बचाने की जुगाड का चिंतन आवश्यक मजबूरी है. यह तो निश्चित रूप से तय है की पर्यावरण बचाने के उपाय उन वैज्ञानिक खोज-औद्योगीकरण-आर्थिक मजबूती के अविभाज्य समीकरण वाले रास्ते से प्राप्त नही होंगे क्योंकी ये उपजे ही उसके कारण है! नये नजरिये से नये उपाय खोजने की नितांत गरज है.यही सही समय भी है.
संमेलन समाप्त, अब आगे क्या?
आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत:!! अर्थात, विश्व भर से अच्छे एवं उपयुक्त विचार हम तक पहुंचे. उपाय की राह की जो चर्चा हम कर रहे है, ऋग्वेद की यह ऋचा उसी ओर इंगित करती है.
इस विश्वंभर (=विश्व भर में व्याप्त) परिस्थिती से निपटने हेतू जनता जनार्दन की सहभागीता एवं सहभाग अनिवार्य है. पर्यावरण से जुडे मुद्दे प्रत्येक देश के राजनीती के मुद्दे बने तो बात जल्दी बनेगी. अत: इस विषय में जन-मत एवं जन-मत के लिए जन-जागरण की अनिवार्यता सिद्ध होती है.
इस संमेलन में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओ को जो पंचामृत प्राशन करवाया है वह अनुठा है. साथ ही उन्होने पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता को अधोरेखित किया है. इस विचार को शीघ्र एक अमली-जामा पहनाना भी एक अभूतपूर्व पहल साबित होगी. हाल ही जारी की गई नवीन शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत इस विषय को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिये. हमेशा की तरह सब कुछ सरकार पर छोडना तो गलत ही होगा.
अब सी.ओ.पी.26 परिषद की बैठक हो चुकी. शीर्ष नेतागण अपने-अपने देश लौट चुके. अगली बैठक तक राम-राम कह चुके! तो क्या इस बार भी, ढाक के वही तीन पात! या फिर, क्या आज से इस बारे में शिक्षाविद, शिक्षक-संघटन स्वयं स्फूर्त प्रयास करेंगे? क्या एन.जी.ओ, सामाजिक संस्था, जन-संघटन, शिक्षा-संस्थान स्वयं-प्रेरणा से ही पर्यावरण के वैश्विक असंतुलन को स्थानिक उपायो से संतुलित करने हेतु जन-जागरण के महा-अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकारेंगे?
ये लेखक के अपने निजी विचार है l