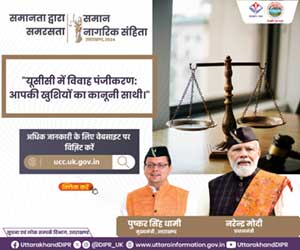नई दिल्ली। भारत ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए चीन द्वारा रखे गए नए नामों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि यह इस ‘निर्विवाद (Undeniable)’ वास्तविकता को बदलने का ‘निरर्थक(Preposterous)’ प्रयास है कि यह राज्य हमेशा भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा।
दरअसल, अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए समय-समय पर नए नामों की सूची जारी करना चीन की पुरानी आदत है। भारत इन नामों को चीन द्वारा खोज बताता है और लगातार और स्पष्ट रूप से इन्हें खारिज करता रहा है।
चीन ने 2017 से ऐसी कई सूचियां जारी की हैं, जिनमें चीनी मंत्रिमंडल के समकक्ष राज्य परिषद द्वारा जारी नियमों के अनुसार नामों को ‘मानकीकृत (Standardise)’ करने का दावा किया गया है।
चीन कब-कब ऐसा किया?
हाल के वर्षों में, यह प्रथा 14 अप्रैल, 2017 को शुरू हुई, जब चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में छह स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नाम जारी किए। उस समय चीनियों ने कहा था कि यह “मानकीकृत” नामों का ‘पहला बैच’ था।
उस सूची में रोमन वर्णमाला में लिखे गए छह नाम ‘वो’ग्याइनलिंग’, ‘मिला री’, ‘कोइडेनगारबो री’, ‘मेनकुका’, ‘बुमो ला’ और ‘नमकपुब री’ थे। नामों के साथ सूचीबद्ध अक्षांश और देशांतर ने उन स्थानों को क्रमशः तवांग, क्रा दादी, पश्चिम सियांग, सियांग (जहां मेचुका या मेंचुका एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है), अंजॉ और सुबनसिरी के रूप में दिखाया – जो अरुणाचल प्रदेश की चौड़ाई में फैले हुए हैं।
साढ़े चार साल बाद, दिसंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए 15 “मानकीकृत चीनी नामों” की “दूसरी सूची” आई। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, इनमें आठ रिहायशी इलाके, चार पहाड़, दो नदियां और एक पहाड़ी दर्रा शामिल थे। इस बार भी चीन ने इन स्थानों के अक्षांश और देशांतर बताए।
2 अप्रैल, 2023 को चीन ने 11 स्थानों के लिए “मानकीकृत भौगोलिक नामों” की तथाकथित “तीसरी सूची” जारी की, जिसमें पांच पर्वत शिखर, दो आबादी वाले क्षेत्र, दो भूमि क्षेत्र और दो नदियाँ शामिल हैं। “पुनः नामित” स्थानों में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नज़दीक एक शहर भी शामिल था।
और पिछले साल चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के लिए ‘नए नामों’ की एक सूची पोस्ट की थी।
सवाल- चीन भारत में स्थित स्थानों का नाम क्यों रख रहा है?
चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है। वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में ‘ज़ंगनान’ कहता है और बार-बार ‘दक्षिण तिब्बत’ का ज़िक्र करता है।
चीनी मानचित्रों में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है, तथा कभी-कभी इसे ‘तथाकथित अरुणाचल प्रदेश’ के रूप में संदर्भित किया गया है।
चीन समय-समय पर भारतीय क्षेत्र पर अपने एकतरफा दावे को रेखांकित करने का प्रयास करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना उसी प्रयास का हिस्सा है।
चीन के दावे का आधार क्या है?
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैकमोहन रेखा की कानूनी स्थिति को लेकर विवाद में है, जो तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है, जिस पर 1914 के शिमला सम्मेलन – जिसे आधिकारिक तौर पर ‘ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन’ कहा जाता है। उसमें सहमति बनी थी।
शिमला सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीन गणराज्य के पूर्णाधिकारी द्वारा किया गया था, जिसे 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद घोषित किया गया था। (वर्तमान साम्यवादी सरकार 1949 में ही सत्ता में आई थी, जब पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई थी।) चीनी प्रतिनिधि ने शिमला कन्वेंशन पर सहमति नहीं जताते हुए कहा कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।
शिमला में मुख्य ब्रिटिश वार्ताकार हेनरी मैकमोहन के नाम पर मैकमोहन रेखा का नाम रखा गया है। यह रेखा भूटान की पूर्वी सीमा से चीन-म्यांमार सीमा पर इसु रजी दर्रे तक खींची गई है। चीन मैकमोहन रेखा के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन अपने दावों का आधार तवांग और ल्हासा के मठों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मानता है।
इन दावों से चीन को क्या मदद मिलेगी?
वह इसे एक तरह की दबाव की रणनीति के रूप में देखता है। यह बीजिंग की व्यापक विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत जब भी कोई भारतीय गणमान्य व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, तो वह नाराजगी भरे बयान जारी करता है।
इसलिए 2017 में नाम बदलने का पहला चरण दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे के कुछ दिनों बाद आया, जिसके खिलाफ बीजिंग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। और 2021 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राज्य विधानसभा में जाने के बाद भी उसने विरोध किया। चीन अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों को वीजा जारी करने में भी मुश्किलें पैदा करता है।
2017 में वांग देहुआ, जो शंघाई में दक्षिण और मध्य एशिया अध्ययन संस्थान के निदेशक थे। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि नाम बदलना चीन में एक सतत प्रक्रिया है, जिस तरह से भारत ने ‘बॉम्बे को मुंबई या मद्रास को चेन्नई ‘ में बदल दिया।
बीजिंग की सरकार अन्य स्थानों को भी अपने चीनी नाम देने की कोशिश करती है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में द्वीप, जिन पर वह संप्रभुता का दावा करता है। वास्तव में, चीन के साथ किए गए कथित ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर क्षेत्रों पर आक्रामक दावे करना चीनी विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है। यह आक्रमण हमेशा चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत के प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित रहता है।